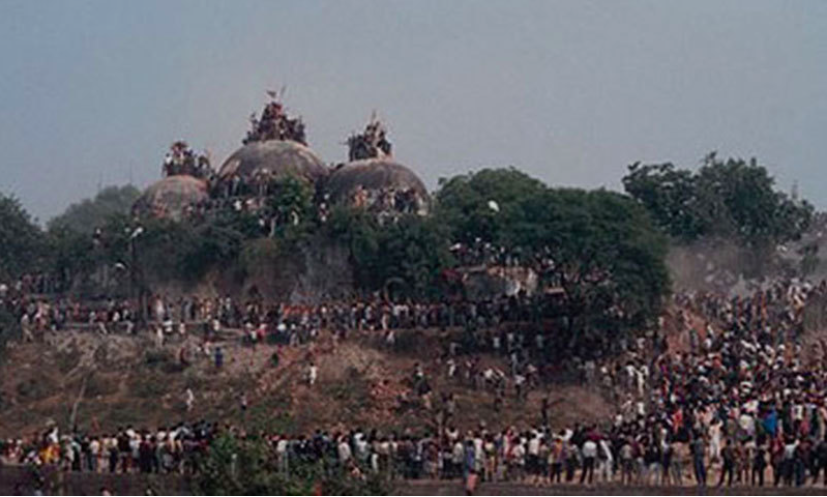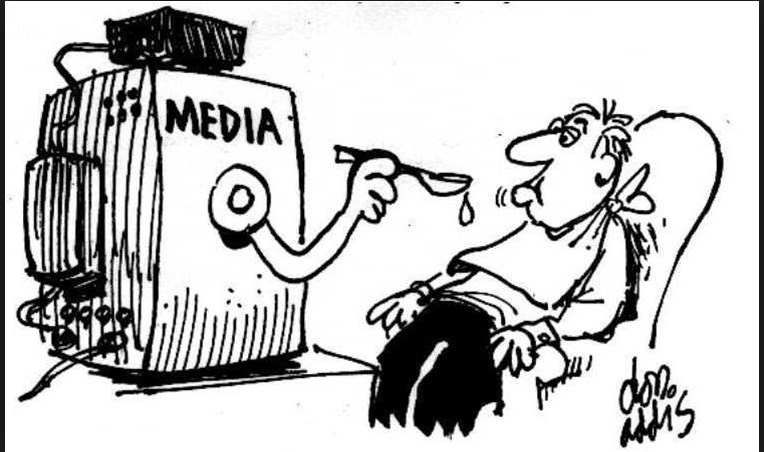संडे मॉर्निंग– सौरभ शाह
कौवापुर और इंटिआठोक के बीच स्थित बलरामपुर स्टेशन नेपाल जानेवाले यात्रियों के लिए विश्राम स्थल का काम करता था. बलरामपुर किसी जमाने में एक छोटी रियासत हुआ करता था. यह नगर घाघरा नदी के किनारे बसा है. १९४७ में यह नगर उत्तरप्रदेश में मिल गया. भारतीय जनसंघ का जन्म आजादी के बाद हुआ. २१ अक्टूबर १९५१ को श्यामाप्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जैसे दिग्गज नेताओं ने भारतीय जनसंघ नाम राजनीतिक दल की स्थापना कर जनता को कांग्रेस का विकल्प दिया.
बलरामपुर की रियासत १९४७ में लोकतंत्र में मिल गया था लेकिन इस प्रदेश से जमींदारी प्रथा अभी दूर नहीं हुई थी. कई जमींदार मुसलमान थे. वे जनता का आर्थिक शोषण तो करते ही थे, लेकिन धार्मिक भेदभाव की भयानक रूप से करते थे.
अटल बिहारी वाजपेयी ने बलरामपुर में चुनाव प्रचार करते हुए देखा कि कई क्षेत्रों में मंदिर में घडियाल और शंख बजाने पर इन मुस्लिम जमींदारों ने प्रतिबंध लगाया था. स्वतंत्रता के बाद इस परिस्थिति में थोडा-बहुत बदलाव आया था लेकिन दूरदराज के प्रदेशों में अब भी परिस्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई थी. छोटे और मध्यम दर्जे के किसानों ने मुस्लिम जमींदारों के आतंक से परेशान होकर जनसंघ को समर्थन देना शुरू कर दिया था. बलरामपुर के लोकसभा चुनाव में वाजपेयी चुनकर आए. यह उनकी पहली चुनावी जीत थी. बलरामपुर निर्वाचन क्षेत्र में कुल ४,८२,८०० मतदाता थे. इसमें से २,२६,९४८ मतदाताओं ने मतदान किया. वाजपेयी को १,१८,२८० वोट मिले थे. कांग्रेस के उम्मीदवार हैदर हुसैन करीब १०,००० वोटों से हारे थे. कांग्रेस ने यदि किसी हिंदू के खडा किया होता तो शायद में वे खुद चुनाव नहीं जीत सकते थे ऐसा वाजपेयी ने स्वयं लिखा है.
लेकिन मथुरा और लखनऊ से वाजपेयी हार गए. मथुरा में तो उनकी जमानत ही जब्त हो गई थी. लखनऊ में जनसंघ का प्रदर्शन अच्छा था. कांग्रेस के विजयी उम्मीदवार पुलिन बिहारी बैनर्जी को ६९,५१९ वोट मिले थे. वाजपेयी को ५७,०३४ वोट मिले. तीसरा उम्मीदवार कम्युनिस्ट पार्टी का था. वाजपेयी ने उल्लेख किया है कि इस कम्युनिस्ट को यदि कुछ ज्यादा वोट मिले होते तो कांग्रेस हार गई होती और जनसंघ को लाभ मिलता. वाजपेयी ने यह भी लिखा है कि जनसंघ को हराने के लिए कम्युस्टिों का समर्थन करनेवालों ने भी कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट देकर जिताया था.
वाजपेयी का यह निरीक्षण आज भी उतना ही सत्य प्रतीत होता है. भाजपा को हराने के लिए विपक्षी `न खेलब, न खेलै देब, खेलवै बिगाडब’ वाली इसी पुरानी कहावत का अनुसरण करते रहे हैं. १९५७ के लोकसभा चुनाव में वाजपेयी सहित जनसंघ के कुल चार उम्मीदवार विजयी हुए थे. १९५७ में लोकसभा के साथ देश के विभिन्न राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी हुए थे, यह ध्यान देने योग्य बात है.
वाजपेयी सहित भारतीय जनसंघ के चारों सांसद पहली बार चुनाव जीते थे. इनमें से किसी भी सांसद को पहले विधानसभा का भी अनुभव नहीं था. संसदीय मार्गदर्शन करनेवाला कोई नहीं था. वाजपेयी को उस समय संसद में अंतिम सीट पर बैठना पडता था. अन्य तीनों साथी उन्हीं के साथ बैठते. लोकसभा अध्यक्ष का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करना एक कठिन काम था. संसद में किसी भी प्रश्न पर चर्चा होती है तो हर सांसद को उनके दल के चुने गए सदस्यों के हिसाब से समय आबंटित किया जाता है. जनसंघ के ४ ही सदस्य होने के कारण वाजपेयी को बोलने के लिए बहुत ही कम समय मिलता था.
वाजपेयी को पहले से ही विदेश नीति में खूब रुचि थी. उस जमाने में जब संसद में अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर चर्चा होती थी तब हर कोई ध्यान से सुनता था. पंडित नेहरू तो प्रधानमंत्री थे ही, विदेश मंत्री भी थे. चर्चा के दौरान जनसंघ के हिस्से में बमुश्किल दो-चार मिनट आते थे. विदेश नीति पर वाजपेयी के पहले संक्षिप्त भाषण ने सभागृह में सभी का ध्यान आकर्षित किया था. सामान्य रूप से विदेश नीति पर अंग्रेजी में चर्चा हुआ करती थी, वाजपेयी ने शुद्ध और धारा प्रवाह हिंदी में संबोधन करके सभी का ध्यान खींचा था.
२० अगस्त १९५८ का दिन था वह. आज से ठीक ५० वर्ष पहले की बात है. प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने विदेश नीति के बारे में चर्चा का अंग्रेजी में विस्तार से जवाब देने के बाद स्पीकर से हिंदी में थोडा बोलने की अनुमति मांगी. सभागृह में उपस्थित सभी सांसदों ने नेहरू के इस प्रस्ताव का तालियों से स्वागत किया. नेहरू ने वाजपेयी का नाम लेकर हिंदी में बोलना शुरू किया और फिर से तालियों की गडगडाहट हुई. नेहरू के इन शब्दों को वाजपेयी ने अपनी स्मृति में अंकित किया है. हम उन शब्दों को यथावत रखकर पढेंगे:
“कल जो बहुत से भाषण हुए उनमें से एक भाषण श्री वाजपेयीजी का भी हुआ. अपने भाषण में उन्होंने एक बात कही थी और ये कहा था कि, मेरे ख्याल में, कि जो हमारी वैदेशिक नीति है, वह उनकी राय में, सही है. मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने यह बात कही. लेकिन एक बात उन्होंने और भी कही कि बोलने के लिए वाणी होनी चाहिए लेकिन चुप रहने के लिए वाणी और विवेक दोनों चाहिए. इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं.”
वाजेपयी उसके बाद के वर्षों में प्रखर वक्ता के रूप में खूब प्रसिद्ध हुए. उनके पास साहसिक वाणी तो थी ही और कब चुप रहना चाहिए, इसका विवेक भी था.
आज का विचार
मैं हमेशा से ही वादे लेकर नहीं आया, इरादे लेकर आया हूं.
– अटल बिहारी वाजपेयी
(मुंबई समाचार, रविवार, १९ अगस्त २०१८)